महान चोल मंदिर
महान चोल मंदिरों का निर्माण चोल राजाओं द्वारा करवाया गया था, जिनका साम्राज्य पूरे दक्षिण भारत और पड़ोसी द्वीपों तक फैला हुआ था। इस स्थल में 11वीं और 12वीं शताब्दी में निर्मित तीन महान मंदिर हैं जिनमें तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, गंगैकोंडचोलीश्वरम का बृहदेश्वर मंदिर, और दारासुरम का एरावतेश्वर मंदिर शामिल हैं। राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए गंगैकोंडचोलीश्वरम मंदिर का निर्माण सन 1035 में पूर्ण हुआ। इसके 53 मीटर के विमान (गर्भगृह शिखर) के आले के समान कोण और भव्य ऊपरी गोलाइयों में गतिशीलता का दृश्य तंजौर के सीधे और ठोस स्तंभ के विपरीत है। दारासुरम का एरावतेश्वर मंदिर परिसर राजराज द्वितीय द्वारा निर्मित किया गया था, और इसमें 24 मीटर का विमान और भगवान शिव की एक पत्थर की मूर्ति विराजमान है। ये मंदिर वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला एवं कांस्य कला के क्षेत्र में चोलों की शानदार उपलब्धि का साक्ष्य प्रदान करते हैं।
उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य
संक्षिप्त संश्लेषण
महान चोल राजवंश ने 9वीं शताब्दी ईस्वी में तंजौर और इसके आस-पास के इलाके में एक शानदार साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने, सैन्य विजय, कुशल प्रशासन, सांस्कृतिक सम्मिलन और कला को बढ़ावा देने जैसे शाही उद्यमों के सारे क्षेत्रों में महान उपलब्धियाँ प्राप्त करते हुए, साढ़े चार शताब्दियों तक लंबा विख्यात शासन किया। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, गंगैकोंडचोलपुरम का बृहदेश्वर मंदिर, और दारासुरम का एरावतेश्वर मंदिर, इन तीनों मंदिरों में आज भी पूजा होती है। हज़ारों सालों से चली आ रही मंदिर की पूजा और अनुष्ठान संबंधी परम्पराएँ, जो उससे भी पहले के आगम ग्रंथों पर आधारित हैं, वे लोगों के जीवन के एक अभिन्न हिस्से के रूप में दैनिक, साप्ताहिक और वार्षिक तौर पर आज भी वैसी ही की जा रही हैं।
इस प्रकार, ये तीन मंदिर परिसर एक विशिष्ट समूह का गठन करते हैं, जो उच्च चोल वास्तुकला और कला के सबसे उच्च स्वरूप के प्रगामी विकास, और साथ ही चोल इतिहास और तमिल संस्कृति की एक बहुत ही विशिष्ट अवधि को प्रदर्शित करते हैं।
तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर चोल वास्तुकारों की सबसे महान उपलब्धि को चिन्हित करता है। अभिलेखों में दक्षिणा मेरू के रूप में प्रसिद्ध, इस मंदिर का शुभारंभ चोल राजा, राजराज प्रथम (सन 985-1012) द्वारा, संभवतः उनके शासनकाल के 19वें वर्ष (सन 1003 -1004) में किया गया था और उन्होंने अपने शासनकाल के 25वें वर्ष (सन 1009-1010) में खुद ही इसका लोकार्पण किया था। इसमें अष्टदिकपालों को समर्पित उप-मंदिरों सहित, एक विशाल स्तंभयुक्त प्रकार और गोपुरा (राजराजंतीरुवसल के नाम से प्रचलित) युक्त मुख्य प्रवेश द्वार है, जिनसे यह विशाल मंदिर घिरा हुआ है। आयताकार प्रांगण के पिछले आधे भाग के मध्य में गर्भगृह स्थित है। विमान ज़मीन से 59.82 मीटर ऊँचा है। इस भव्य ऊँची संरचना में एक उच्च उप-पीठ, और मोटी पट्टियों सहित एक अधिष्ठान बना हुआ है; ज़मीनी स्तर (प्रस्तर) दो स्तरों में विभाजित है, जिसमें भगवन शिव की मूर्तियाँ बनी हुईं हैं। इसके ऊपर 13 तल हैं और उनके ऊपर आठ कोनों वाला शिखर है। गर्भगृह के अंदर एक विशाल लिंग स्थापित है। गर्भगृह के चारों तरफ एक प्रदक्षिणा पथ है। मंदिर की दीवारों को विशाल और उत्कृष्ट भित्ति चित्रों से सजाया गया है। गर्भगृह के चारों ओर द्वितीय भूमि की दीवारों पर, एक सौ आठ करणों में से इक्यासी करण, भरतनाट्य की मुद्रा में तराशे गए हैं। अम्मान को समर्पित 13वीं शताब्दी का एक मंदिर भी है।
मंदिर परिसर के बाहर, एक खंदक से घिरी शिवगंगा छोटे क़िले की दीवारें और शिवगंगा जलाशय है जिसे चोल राजवंश के उत्तराधिकारी और 16वीं शताब्दी के तंजौर के नायकों ने बनवाया था। किले की दीवारों के भीतर ही यह मंदिर परिसर सुरक्षित रूप से स्थित है, और ये दीवारें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा हैं।
पेरम्बलूर जिले में गंगैकोंडचोलपुरम के भगवान शिव को समार्पित बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना राजेंद्र प्रथम (सन 1012-1044) द्वारा की गई थी। इस मंदिर में अद्भुत गुणवत्ता वाली मूर्तियाँ मौजूद हैं। भोगशक्ति और सुब्रह्मण्य की कांस्य मूर्तियाँ चोल धातु मूर्तिकला की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं। आठ देवताओं वाली कमल वेदिका, सौरपीठ (सौर वेदिका) को शुभ माना जाता है।
तंजौर का एरावतेश्वर मंदिर चोल राजा राजराज द्वितीय (सन 1143-1173) द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर आकार में तंजौर और गंगैकोंडचोलपुरम के बृहदेश्वर मंदिरों की तुलना में बहुत छोटा है। इस मंदिर में इन दोनों मंदिरों के मुकाबले कहीं अधिक अलंकरण है। इस मंदिर में गर्भगृह के साथ कोई प्रदक्षिणा पथ और अक्षीय मंडप नहीं हैं। अग्रभाग वाला मंडप, जो अभिलेखों में राजगंभीरन तिरूमंडपम के नाम से उल्लेखित है, एक अनोखा मंडप है, जिसकी संकल्पना एक पहियों वाले रथ के रूप में की गई थी। इस मंडप के स्तंभ भरपूर रूप से अलंकृत हैं। मूर्तियों से सजी वास्तुकला सहित, इस मंदिर की सभी इकाइयों का उत्थान सुंदर है। इस मंदिर की कुछ मूर्तियाँ चोल कला की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं। 63 नयनमारों (शैव संतों) के साथ हुई घटनाओं को उजागर करने वाली अंकितक लघु चित्र वल्लरियाँ उल्लेखनीय हैं और इस क्षेत्र में शैव पंथ की गहरी जड़ों को प्रदर्शित करती हैं। मुख्य मंदिर के निर्माण के कुछ समय बाद, देवी के लिए एक अलग मंदिर का निर्माण, दक्षिण भारतीय मंदिर परिसर के एक आवश्यक अंग के रूप में अम्मान मंदिर के उद्भव को प्रकट करता है।
मानदंड (i): दक्षिण भारत के ये तीन चोल मंदिर, द्रविड़ शैली के मंदिरों के शुद्ध रूप की स्थापत्य अवधारणा में एक उत्कृष्ट रचनात्मक उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं।
मानदंड (ii): तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर चोल मंदिरों का पहला महान उदाहरण बना, जिसके निर्माण के बाद अन्य दो स्थलों का भी विकास हुआ।
मानदंड (iii): ये तीन महान चोल मंदिर चोल साम्राज्य की वास्तुकला और दक्षिणी भारत में तामिल सभ्यता के विकास के असाधारण और सबसे उत्कृष्ट प्रमाण हैं।
मानदंड (iv): तंजौर, गंगैकोंडचोलपुरम, और दारासुरम के महान चोल मंदिर वास्तुकला और चोल विचारधारा के प्रतिनिधित्व के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।
समग्रता
ये मंदिर, चोल काल से लेकर मराठा काल तक द्रविड़ वास्तुकला के विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये तीनों स्मारक, इस स्थल के नामांकन के समय से लेकर अब तक संरक्षण की एक अच्छी स्थिति में हैं और कोई भी बड़ा खतरा इन विश्व धरोहर स्मारकों को प्रभावित नहीं कर रहा है। इन स्मारकों का रखरखाव और इनकी निगरानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की जाती है। हज़ारों सालों पहले स्थापित इन मंदिरों में आराधना और अनुष्ठान की परंपराएँ, जो उससे भी पहले के आगम ग्रंथों पर आधारित हैं, लोगों की ज़िन्दगी के एक अभिन्न हिस्से के रूप में आज भी दैनिक, साप्ताहिक और वार्षिक तौर पर जारी हैं।
प्रामाणिकता
इन तीनो स्थलों की, उनकी संकल्पना, सामग्री और कार्यान्वयन के संबंध में, प्रामाणिकता स्थापित है। ये मंदिर अभी भी उपयोग में हैं, और उनके महान पुरातात्विक और ऐतिहासिक मूल्य हैं। ये मंदिर परिसर प्रमुख शाही शहरों का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आज मुख्य रूप से ग्रामीण संदर्भ में उत्कृष्ट विशेषताओं के रूप में स्थापित हैं। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर परिसर के भागों को 1987 में विश्व धरोहर संपत्ति घोषित किया गया, जिसमें छह उप-मंदिर भी शामिल हैं जिन्हें समय के साथ मंदिर के प्रांगण में बाद में जोड़ा गया था। बाद में किए गए परिवर्धन और हस्तक्षेप, इसकी समरूपता और समग्र अखंडता को ध्यान में रखते हुए, मुख्य मंदिर परिसर में सन्निहित मूल अवधारणा को सुदृढ़ करते हैं। आराधना और अनुष्ठान के लिए मंदिर का पारंपरिक उपयोग इसकी प्रामाणिकता में योगदान देता है। हालांकि 2003 की आवधिक रिपोर्ट में संरचनाओं की रासायनिक सफाई और मंदिर के फ़र्श का पूर्ण रूप से प्रतिस्थापन जैसे कई संरक्षण हस्तक्षेपों की ओर ध्यान खींचा गया है जो संरचनाओं की प्रामाणिकता पर गहरा असर डाल सकते हैं। इससे संपत्ति के संरक्षण को निर्देशित करने के लिए एक संरक्षण प्रबंधन योजना की आवश्यकता सामने आई है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मंदिर परिसरों की प्रामाणिकता बनी रहे।
इसी प्रकार, गंगैकोंडचोलपुरम के बृहदेश्वर मंदिर परिसर में, चंदेसा और अम्मान उप-मंदिर मूल रूप से राजेंद्र प्रथम और साथ ही सिंहकेनी (सिंह-कुआँ) की योजना के अनुसार बनाए गए थे। समय के साथ थेंनकैलाश, गणेश और दुर्गा उप-मंदिरों को जोड़ा गया। इन परिवर्धनों की प्रामाणिकता, आगम ग्रंथों में मौजूदा मंदिरों के नवीनीकरण और पुन:निर्माण संबंधी निर्देशों द्वारा समर्थित है।
दारासुरम में, राजपत्र के बाद से पुरातात्विक साक्ष्य संपत्ति की प्रामाणिकता को और बढ़ा देते हैं। अकेला एरावतेश्वर मंदिर ही ऐसा मंदिर है, जिसे बिना किसी अतिरिक्त संरचनाओं के साथ एक ही समय पर बनाया गया है, और वह आज तक अपने मूल रूप में ही मौजूद है। एरावतेश्वर मंदिर के निर्माण के कुछ समय बाद निर्मित देवनायकी अम्मान मंदिर भी अपनी परिसीमा के भीतर अपने मूल रूप में स्थित है।
संरक्षण और प्रबंधन आवश्यकताएँ
तीनों सांस्कृतिक स्थल, अर्थात तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर परिसर, गंगैकोंडचोलपुरम का बृहदेश्वर मंदिर परिसर, और दारासुरम का एरावतेश्वर मंदिर परिसर क्रमशः 1922, 1946 और 1954 से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में हैं। इसके अलावा, ये तीनों मंदिर, वर्ष 1959 में जारी होने के समय से, तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम के अधीन हैं। इसलिए, इन सांस्कृतिक संपत्तियों के प्रबंधन को दो अलग-अलग भागों में विभाजित किया जा सकता है: (1) भौतिक संरचना, वास्तुकला और स्थल की विशेषताओं, पर्यावरण और परिवेश, चित्रकारियों, मूर्तियों और अन्य अवशेषों सहित संपत्तियों का संरक्षण, मरम्मत और रखरखाव; तथा (2) कर्मचारी प्रारूप और पदानुक्रम, लेखा और बहीखाता, लेख पत्र और नियमों सहित मंदिर प्रशासन। भाग (1) के संबंध में प्रबंधन प्राधिकरण पूरी तरह से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास है, जबकि भाग (2) में शामिल पहलुओं की देखभाल पूरी तरह से तमिलनाडु सरकार के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग द्वारा किया जाता है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि संपत्ति का प्रबंधन, इन दो संस्थाओं, एक केंद्रीय और दूसरी राजकीय संस्था द्वारा, संयुक्त रूप से किया जाता है।
इन दो संस्थाओं की कार्यप्रणाली में उनकी प्रबंधन योजनाओं को स्वतंत्र रूप से तैयार करना और समय-समय पर उनकी समीक्षा करना शामिल है। जब आवश्यक होता है, तब संयुक्त विचार-विमर्श किया जाता है और किसी भी स्पष्ट विरोधाभास या संघर्ष के मुद्दों पर उचित विचार किया जाता है और उन्हें हल किया जाता है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर और दारासुरम के एरावतेश्वर मंदिर के मामलों में, ये संस्थाएं किसी भी ऐसे मुद्दे को अंतिम रूप देने से पहले राजभवन देवस्थानम के वंशानुगत ट्रस्टी से परामर्श करती हैं, जिसमें ट्रस्टी के विचार लेना आवश्यक होता हो।
हालाँकि, विस्तारित संपत्ति के नामांकन के बाद से, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, और तमिलनाडु सरकार के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग, संपत्ति प्रबंधन योजना का एक ही मिला-जुला मसौदा तैयार करने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए हैं। इसमें न केवल दोनों पक्षों की विशिष्ट आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाएगा बल्कि तीनों सांस्कृतिक संपत्तियों की रक्षा और संवर्धन के सबंध में मूलभूत उद्देश्यों की पूर्ती भी की जाएगी, जिनमें (1) उनके उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य; (2) वैदिक और आगमिक परंपराओं और लोगों के जीवन में उनके महत्व; (3) कला (मूर्तिकला, चित्रकला, कांस्य कला, नृत्य, संगीत, और साहित्य) जैसे पारंपरिक अविभाज्य संस्कृति घटकों; तथा (4) वास्तु और शिल्प शास्त्रों के प्राचीन विज्ञान, मंदिरों और धार्मिक संरचनाओं के निर्माण और मूर्तिकला और चित्रकला हेतु मूलभूत दिशानिर्देशों, को बढ़ावा देना शामिल होगा।
संपत्ति को विश्व धरोहर संपत्ति घोषित करने के बाद से, स्मारकों को अच्छी दशा में संरक्षित रखा गया है और इनको किसी भी प्रकार से कोई हानि होने का खतरा नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इन स्मारकों का रखरखाव और समय-समय पर इनकी जाँच की जाती है, जिससे ये स्मारक, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। हालाँकि, आगामी कार्यों के दिशानिर्देश हेतु एक पर्यटन प्रबंधन और विवेचन योजना और संरक्षण प्रबंधन योजना आवश्यक है, जो संरक्षण और विवेचन के प्रयास के लिए प्राथमिकताएँ निर्धारित कर सके। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जगह-जगह पर पीने का पानी, शौचालय, आदि, जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। दीर्घकालिक योजनाओं में भूनिर्माण और पर्यटकों की सुविधाओं में सुधार जैसी योजनाएँ भी शामिल हैं। ये मंदिर पिछले 800-1000 वर्षों से आस्था के केंद्र रहे हैं और आगे भी ऐसे ही बने रहेंगे। आगंतुकों की संख्या और इसके प्रभावों की निगरानी आवश्यक है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस संपत्ति के अद्भुत सार्वभौमिक मूल्य को कोई खतरा ना पैदा हो।
अद्भुत जीवंत चोल मंदिर उन तीन मंदिरों का समूह है, जिनका निर्माण नौवीं से बारहवीं शताब्दी के बीच दक्षिणी भारत पर शासन करने वाले चोल राजाओं द्वारा कराया गया था। इन तीन मंदिरों में तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, गंगैकोंडचोलपुरम का बृहदेश्वर मंदिर, और दारासुरम का एरावतेश्वर मंदिर शामिल हैं। इनमें से, सर्वप्रथम तंजावुर के मंदिर को, द्रविड़ वास्तुकला और चोल मूर्तियों का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व करने के लिए, वर्ष 1987 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। बाद में इसी तरह की स्थापत्य प्रतिभा और मूर्तियों और चित्रकारियों के रूप में चोल कला के प्रतिनिधित्व के लिए, अन्य दो स्थलों को भी वर्ष 2004 में विश्व विरासत घोषित किया गया।
तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को चोल राजा राजराज प्रथम ने नौवीं शताब्दी में बनवाया था और इसे भगवान शिव को समर्पित किया था। इसे राजराजेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका नाम स्वयं सम्राट के नाम पर रखा गया था। यह मंदिर पूर्णतया ग्रेनाइट से निर्मित होने वाले प्रारंभिक मंदिरों में से एक था। चूँकि ग्रेनाइट स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं था इसलिए इसे बाहर से लाया गया था। जो बात बृहदीश्वर मंदिर को विशिष्ट बनाती है, वह है इसका 59.82 मीटर ऊँचा विमान, जो कि मुख्य मंदिर (गर्भ-गृह) के ऊपर स्थापित है। यह एकमात्र मंदिर है जिसका विमान, गोपुरम (प्रवेश द्वार) की तुलना में लंबा है और यह द्रविड़ वास्तुकला में एक असामान्य बात है।
वास्तुकला के अलावा, मंदिर अपने शिलालेखों, मूर्तियों और चित्रकारियों के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर की दीवारों पर शिव, विष्णु, गणेश, दुर्गा जैसे देवी-देवताओं के साथ-साथ द्वारपालों की नक्काशी की गई है।
गंगैकोंडचोलपुरम में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण; तंजावुर में मंदिर का निर्माण कराने वाले शासक राजराज प्रथम के पुत्र राजेंद्र प्रथम द्वारा कराया गया था। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर सोमस्कंद, कार्तिकेय और भोग-शक्ति-देवी जैसी सर्वश्रेष्ठ चोल कांस्य मूर्तियों के लिए जाना जाता है। इसमें नवग्रह या नौ ग्रहों वाला एक अद्वितीय खंड भी है, जो दर्शाता है कि सम्राट उत्तरी और दक्षिणी तत्वों को संयोजित करने हेतु कितने प्रयत्नशील थे।
तीसरा मंदिर एरावतेश्वर मंदिर है, जिसे, राजाराजेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध, चोल राजा राजराज द्वितीय ने बारहवीं शताब्दी में बनवाया था। एक किंवदंती के अनुसार, राजा एक ग्वालिन की इच्छा को पूरा करने के लिए दारासुरम में एक मंदिर का निर्माण करना चाहते थे। उस महिला ने तंजावुर के मंदिर में उपयोग के लिए एक बड़ा पत्थर उपहार में दिया था और बदले में, उसकी इच्छा थी कि उसके गाँव में एक मंदिर बनाया जाए। यह मंदिर अपनी भव्यता और शैली के लिए प्रसिद्ध, बाकि दो मंदिरों की तुलना में आकार में छोटा, अधिक जटिल और अलग है। एरावतेश्वर मंदिर में स्थापित रथ के आकार में बनाया गया राजगम्भीरम थिरुमंडपम, इसकी खास विशेषताओं में से एक है, जिसके निचले हिस्से में नक्काशी किए गए घोड़े हैं जिससे आभास होता है कि रथ को खींचा जा रहा है। यह माना जाता है कि शिव ने त्रिपुरान्तक (शिव की एक अभिव्यक्ति) के रूप में इस रथ की सवारी की थी।ये तीनों मंदिर इस बात का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं कि किस प्रकार से चोल वास्तुकला और मूर्तिकला का उद्भव और समय के साथ विकास हुआ।
 भारत सरकार
भारत सरकार




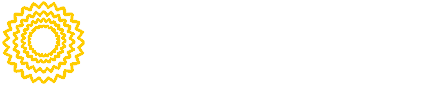 डिजिटल भविष्य के लिए स्वयं को तैयार करने की आवश्यकता को पहचानते हुए, ‘भारतीय संस्कृति’ पोर्टल, संस्कृति मंत्रालय द्वारा एक पहल है। यह एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो पूरे भारत की विभिन्न रिपॉज़िटरियों और संस्थानों से सांस्कृतिक प्रासंगिकता के डेटा को प्रस्तुत करता है।
डिजिटल भविष्य के लिए स्वयं को तैयार करने की आवश्यकता को पहचानते हुए, ‘भारतीय संस्कृति’ पोर्टल, संस्कृति मंत्रालय द्वारा एक पहल है। यह एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो पूरे भारत की विभिन्न रिपॉज़िटरियों और संस्थानों से सांस्कृतिक प्रासंगिकता के डेटा को प्रस्तुत करता है।
